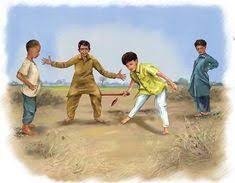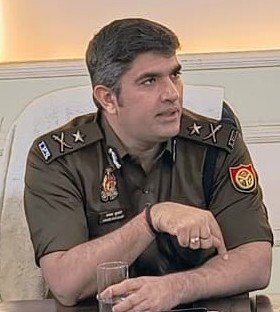झांसी,04 दिसंबर। पिछले दिनों एक हमख्याल मित्र और वाट्सएप की वजह से कुछ प्यारी सी बाल कवितायें फिर नज़रों के सामने से गुज़रीं – “ यदि होता किन्नर नरेश मैं ”, “ हठ कर बैठा चाँद एक दिन माता से यह बोला”. लगा जैसे हमारे बचपन को जोड़ने वाला कोई रज्जु मार्ग खुल गया हो।

अतीत से आज के दरमियान तापों – संतापों, दंशों – भ्रंशों, नाकामियों – नाफ़रमानियों, ठहरावों – संघर्षों का इतना लंबा बीहड़ उग आया है कि बालपन के दिनों से नाता टूट सा गया है। विशेषकर उन दिनों की अपनी विशिष्ट मनःस्थितियों पर सोचने का वक़्त ही नहीं मिलता है जबकि हमारी मानसिक बनावट की बुनियादी ईंटें उसी समय रखी जा रही थी।
हमारा बचपन कस्बाई था। वस्तुएं थोड़ी कम थी, बाज़ार का दायरा छोटा था, रोज़मर्रा की चीज़ों के आपसी लेन- देन का दायरा ज़्यादा बड़ा था, सूई से लेकर खटिया – बिस्तर तक के व्यवहार में शर्म की कोई जगह नहीं थी। इन्हीं छोटी मोटी- चीज़ों के साथ भावनाएँ – भरोसे भी बिना शोर किये किये एक आँगन से दूसरे आँगन तक आवाजाही करते थे। हम बच्चे पैदा अपने घर में हुए लेकिन पले- बढ़े कई -कई आँगनों में। आँगनों के फर्श की ऊँच – नीच उस समय भी थी , लेकिन भरोसे की अबाध आवाजाही ने हम बच्चों तक उस उच्चावच को पहुँचने नहीं दिया। कभी कभी सोचता हूँ कि आजकल की तरह सामाजिक व जातीय खेमाबंदी अगर होती, तो हम भी आज की पीढ़ी की तरह ही शंकालु होते, सहमे से होते, इंसानों से ज़्यादा मशीनों पे भरोसा करने वाले होते। लिहाज़ा यह कहा जा सकता है कि कोई पीढ़ी दोषी नहीं होती , दोषी उसे गढ़ने वाली सामाजिक दशाएं होती हैं।
बहरहाल बात उन दिनों की हो रही थी; तब तक शिक्षा और व्यवसाय पर्यायवाची शब्द नहीं हुए थे, बच्चों के पाठ्यक्रम उलझे नहीं थे, आज की तरह बाल मन मशीनी आडम्बरों, प्रोजेक्ट वर्कों आदि में उलझा नहीं था। पढ़ाई की पहली सीढ़ी अपनी भाषा और बाल सुलभ साहित्य था। छोटी छोटी मन भावन कविताएं व कथाएं मन में ऐसा रस घोलती थीं कि उनकी छाप आज तक अमिट है। शब्दावली ऐसी कि घर पर ही पांचवीं पास दादी या माँ सहजता से समझा दें। मसलन – “अम्मा ज़रा देख तो ऊपर / चले आ रहे हैं बादल..”, ‘4उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो’’, “ सूरज निकला चिड़ियाँ बोलीं, कलियों ने भी आंखें खोलीं ”…. अध्यापक केवल विद्यालय तक ही नहीं बल्कि घरों – बाज़ारों तक अध्यापक की ही भूमिका में थे और जब जी चाहा पूरे अधिकार भाव से जी भरकर इस बात की पुष्टि भी कर देते थे।
आज भी उनके व्यक्तित्व अपनी पूरी आभा और आतंक के साथ स्मृति में दर्ज़ हैं। इन्हीं स्मृतियों ने हमारी शख्सियत को उन राज मार्गों की शक्ल दे दी जिन पर विचारों के चेकपोस्ट भी हैं, भावनाओं के विश्राम गृह भी हैं। वर्तमान को जब मैं देखता हूँ तो कांप उठता हूँ कि हम कैसी पीढ़ी गढ़ रहे हैं कि जिसके पास न विचारों के लिए वक़्त है , जो न भावनाओं की शीतल छाया में रुकना चाहती है; यहां केवल और केवल रफ्तार है। ऐसी अंधी गति जिसे सामने अगल बगल किसी की परवाह नहीं। ऐसे नॉन थिंकिंग और बेलगाम समाज के एक्सीडेंट कितने ख़तरनाक होते हैं, हम सब रोज़ सुनते गुनते हैं। अगर पलक झपकते ही बड़े पैमाने पर जान माल की हानि आम सी लगने वाली घटना हो गयी है, तो इसके मूल में कहीं न कहीं हृदय की उस भाव सम्पदा का क्षरण भी जिम्मेदार है, जिसे भाषा और अनुभव के मधुर अद्वैत से हमने अपने बालपनों में अर्जित किया था।
आज टी वी, मोबाइल और सोशल मीडिया के शोर और चकाचौध से घिरा बाल मन कहाँ रग्घू कुम्हार के घर के पास रुक कर चाक चलते देखना चाहेगा ( वैसे अब रग्घू कुम्हार भी दुर्लभ जीव है ), अम्मा से बारिश में भींगने की ज़िद करेगा या सावन और डाल पर झूले का मतलब समझेगा। किन्नर नरेश होना तो अब उसकी कल्पनाओं के पाठ्यक्रम में ही नहीं रहा। जब कल्पनायें अपने सुदूर अतीत से कट जाती हैं और अपनी स्मृतियों से बिछुड़ जाती हैं तो, या तो बाज़ारू बनती हैं या विस्फोटक। दोनों ही स्थितियों में सामाजिकता नष्ट होती है। तो क्या हम पुनः समाजविहीन पशुता की अवस्था में लौटने वाले हैं ?
राहुल मिश्रा,
प्रवक्ता, राजकीय इंटर कालेज